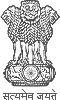मानव-जनित आपदा
जैविक आपदा
जैविक आपदाएँ कार्बनिक उत्पत्ति की प्रक्रियाओं या जैविक वाहकों द्वारा संचरित घटनाओं के कारण होती हैं। इनमें रोगजनक सूक्ष्मजीवों, विषाक्त पदार्थों और जैव सक्रिय पदार्थों के संपर्क शामिल होते हैं, जो जीवन की हानि, चोट, बीमारी या अन्य स्वास्थ्य प्रभाव, संपत्ति की क्षति, आजीविका और सेवाओं की हानि, सामाजिक और आर्थिक अव्यवस्था या पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकते हैं।
जैविक आपदाओं के उदाहरणों में महामारी रोगों के प्रकोप, पौधों या पशुओं में संक्रामक रोग, कीटों या अन्य जानवरों की बाढ़ और संक्रमण शामिल हैं। जैविक आपदाएँ निम्न रूपों में हो सकती हैं:
- महामारी (Epidemic): किसी जनसंख्या, समुदाय या क्षेत्र में एक ही समय पर असामान्य रूप से बड़ी संख्या में व्यक्तियों को प्रभावित करना। उदाहरण: हैजा, प्लेग, जापानी इंसेफेलाइटिस (JE)/ तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES)।
- महामहामारी (Pandemic): एक महामारी जो एक बड़े क्षेत्र (महाद्वीप या पूरे विश्व) में फैल जाती है, जिसमें मौजूदा, उभरते या पुनः उभरते रोग और संक्रामक रोग शामिल होते हैं। उदाहरण: इन्फ्लुएंजा H1N1 (स्वाइन फ्लू)।
रासायनिक आपदा
रसायन आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के मूल में होते हैं और उन्होंने सरकार, निजी क्षेत्र और समुदाय के भीतर आपदा प्रबंधन के लिए गंभीर चिंताएँ उत्पन्न की हैं। रासायनिक आपदाओं का मानव पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे जनहानि और प्रकृति एवं संपत्ति की क्षति हो सकती है।
रासायनिक आपदाओं में उच्चतम जोखिम वाले तत्व औद्योगिक संयंत्र, कर्मचारी और श्रमिक, खतरनाक रसायनों के वाहन, आस-पास की बस्तियों के निवासी, समीपवर्ती भवन, उनके निवासी और आसपास का समुदाय होते हैं।
रासायनिक आपदाएँ कई तरीकों से उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे:
- प्रक्रिया और सुरक्षा प्रणालियों की विफलता
- मानव त्रुटियाँ
- तकनीकी त्रुटियाँ
- प्रबंधन संबंधी त्रुटियाँ
- प्राकृतिक आपदाओं के प्रेरित प्रभाव
- परिवहन के दौरान दुर्घटनाएँ
- खतरनाक अपशिष्ट का प्रसंस्करण/निपटान
- आतंकी हमले/अशांति जिसके कारण तोड़फोड़
भारत में रासायनिक आपदा जोखिम की स्थिति
भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी रासायनिक (औद्योगिक) आपदा — “भोपाल गैस त्रासदी” 1984 में देखी। यह दुर्घटना इतिहास की सबसे विनाशकारी रासायनिक घटना थी, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) नामक विषैली गैस के आकस्मिक रिसाव के कारण हुई।
भोपाल के बाद भी, भारत में लगातार रासायनिक दुर्घटनाएँ होती रही हैं। केवल पिछले एक दशक में ही 130 बड़ी रासायनिक दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें 259 मौतें और 563 गंभीर चोटें हुईं।
देशभर में लगभग 1861 प्रमुख दुर्घटना जोखिम (MAH) इकाइयाँ फैली हुई हैं, जो 25 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 301 जिलों में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, हजारों पंजीकृत और अपंजीकृत कारखाने खतरनाक पदार्थों से निपटते हैं, जो गंभीर आपदा जोखिम उत्पन्न करते हैं।
भारत में रासायनिक जोखिम को संबोधित करने के लिए उठाए गए सुरक्षा उपाय
भारत में एक व्यापक कानूनी और संस्थागत ढांचा मौजूद है। कई नियम परिवहन, दायित्व, बीमा और मुआवजे में सुरक्षा को कवर करते हैं।
प्रासंगिक प्रावधान:
- विस्फोटक अधिनियम, 1884
- पेट्रोलियम अधिनियम, 1934
- कारखाना अधिनियम, 1948
- कीटनाशक अधिनियम, 1968
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988
- लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
भारत सरकार ने रासायनिक सुरक्षा और दुर्घटना प्रबंधन के कानूनी ढांचे को नए नियम लागू करके और मजबूत किया है, जैसे:
- MSIHC नियम
- EPPR नियम
- SMPV नियम
- CMV नियम
- गैस सिलेंडर नियम
- खतरनाक अपशिष्ट नियम
- गोदी श्रमिक नियम
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने रासायनिक आपदा प्रबंधन पर विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश मंत्रालयों, विभागों और राज्य प्राधिकरणों को विस्तृत आपदा प्रबंधन योजनाएँ तैयार करने की दिशा प्रदान करते हैं।
इन दिशानिर्देशों में विभिन्न स्तरों पर तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए सक्रिय, सहभागी, बहु-विषयक और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। NDMA भविष्य की रासायनिक आपदाओं से बचाव के लिए कानूनी संशोधनों और मुख्य कारखाना निरीक्षकालय (CIFs) को मजबूत करने के सुझाव